वंदे मातरम् के 150 वर्ष : भारत की आत्मा का उद्घोष
08 Nov 2025 13:23:14
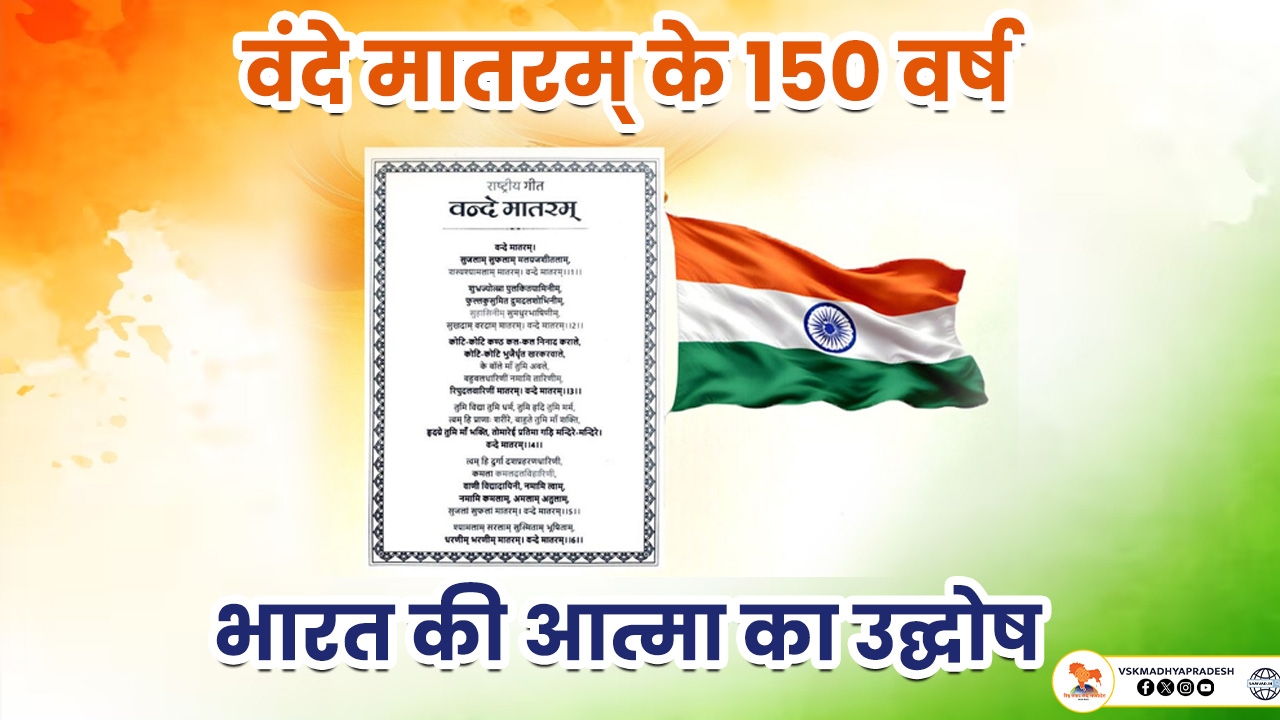
-डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे
भारत के राष्ट्रीय जीवन में कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो युगों को पार करते हुए भावनाओं की ज्योति बन जाते हैं। “वंदे मातरम्” ऐसा ही एक प्रतीक है। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का उद्घोष है।
जब बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा, तब यह गीत भारत के दासत्व के अंधकार में दीपशिखा बनकर प्रकट हुआ। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन था, आत्मविश्वास टूटा हुआ था और जनता को एक सूत्र में बाँधने के लिए किसी चेतना-प्रतीक की आवश्यकता थी।
“वंदे मातरम्” उस कालखंड की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा घोष बना।
बंकिमचंद्र का भावलोक : राष्ट्र की माता का दर्शन
1870 के दशक में जब बंकिमचंद्र ने “आनंदमठ” लिखा, तब उन्होंने भारतमाता को ‘दुर्गा’ के रूप में देखा, जो दैवी स्वरूप के बजाय देश की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी।
वंदे मातरम् का “सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्” केवल कविता नहीं, भारत के प्राकृतिक वैभव का सांस्कृतिक चित्रण है। यह भूमि, जल, वायु, वन और अन्न का स्तवन है, जो किसी धार्मिक आराधना से ऊपर जाकर सम्पूर्ण मानवता को समर्पित है।
स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम् की भूमिका
स्वतंत्रता आंदोलन का हर चरण “वंदे मातरम्” की गूंज से आलोकित था। 1905 में बंग-भंग आंदोलन के समय यह गीत जन-प्रतिरोध का नारा बना। महात्मा गांधी, अरविन्द घोष, बिपिनचंद्र पाल, लाला लाजपत राय और सुभाषचंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने इसे राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना।
1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जब यह गीत गाया गया, तब पूरा हॉल “वंदे मातरम्” के स्वर से गूंज उठा, मानो भारतमाता स्वयं जाग उठी हो।
वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, आंदोलन की आत्मा था।
जलियांवाला बाग में गोली खा रहे युवाओं के होंठों पर, भगतसिंह के जयघोष में और नेताजी के “जय हिन्द” के साथ यह गीत भारत की पहचान बन गया।
वंदे मातरम् और संविधानिक मान्यता
भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने इसकी राष्ट्रीय भूमिका को स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में निर्णय हुआ कि “जन गण मन” राष्ट्रीय गान होगा और “वंदे मातरम्” को समान आदर के साथ राष्ट्रीय गीत का स्थान दिया जाएगा। इस प्रकार यह भारत की आत्मा और पहचान दोनों का प्रतीक बना।
विरोध का नरेटिव : अस्मिता पर प्रहार
आज कुछ राजनीतिक और धार्मिक समूह “वंदे मातरम्” का विरोध करते हुए यह नरेटिव गढ़ते हैं कि यह केवल हिंदू देवी की स्तुति है। वे भूल जाते हैं कि यह भारत की भूमि और मातृत्व का प्रतीक है, न कि किसी मजहबी पूजा-पद्धति का। वास्तव में यह विरोध भारत की राष्ट्रीय एकता और अस्मिता के विरुद्ध है। जो “वंदे मातरम्” का विरोध करता है, वह भारत के मातृत्व भाव और राष्ट्रीयता का विरोध करता है।
उनके इस नरेटिव को तथ्यों से तोड़ा जा सकता है -
• “वंदे मातरम्” में कहीं भी किसी संप्रदाय का उल्लेख नहीं है।
• यह गीत वैदिक दृष्टि से “माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्याः” की भावना को प्रतिध्वनित करता है।
• बंकिमचंद्र स्वयं समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे, न कि संकीर्ण धार्मिक विचारक।
विरोध के ऐतिहासिक और समसामयिक उदाहरण
“वंदे मातरम्” का विरोध नया नहीं है। यह समय-समय पर उन शक्तियों ने किया है जो भारत की अखंडता और अस्मिता के मूल भाव से असहज रही हैं।
1905 – बंग-भंग आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने “वंदे मातरम्” का विरोध किया, यह कहते हुए कि इसमें “हिंदू देवी” का उल्लेख है।
1937 – जब कांग्रेस सरकारों ने विद्यालयों में इसे गाने की परंपरा शुरू की, तब मुस्लिम लीग ने विरोध किया और छात्रों को बहिष्कार का निर्देश दिया।
1947 के बाद – पाकिस्तान के गठन के बाद भी अलगाववादी संगठनों ने भारत में इसके सार्वजनिक गायन को “मजहबी असहिष्णुता” बताया।
2006 – वंदे मातरम् के 125 वर्ष पूरे होने पर कुछ मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे गाने से इनकार किया।
2022–2024 – कुछ राज्यों में नगर निगमों और विधानसभाओं में इसे गाने का विरोध किया गया तथा “अनिवार्य न गाने” की अपील तक की गई।
इन घटनाओं से स्पष्ट है कि विरोध धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। इसका उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना और भारत की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करना था।
नरेटिव को तोड़ने की दिशा : अस्मिता का पुनर्पाठ
विरोधियों का यह कथानक कि “वंदे मातरम्” सांप्रदायिक है, भारत के सांस्कृतिक स्वरूप की अज्ञानता का परिणाम है।
इस झूठे नरेटिव को समाप्त करने के लिए तीन स्तरों पर कार्य आवश्यक है —
ऐतिहासिक स्तर पर – यह तथ्य सार्वजनिक करना कि यह गीत किसी धर्म का नहीं, बल्कि राष्ट्र-भक्ति आंदोलन का प्रेरणास्रोत था।
शैक्षिक और सांस्कृतिक स्तर पर – विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में “वंदे मातरम्” के अर्थ, प्रतीक और इतिहास को पढ़ाया जाए।
राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर – विभाजनकारी नरेटिव का वैचारिक प्रतिवाद किया जाए।
‘वंदे मातरम्’ विभाजन का नहीं, एकता का घोष है। यह किसी धर्म का नहीं, सम्पूर्ण मानवता का जयगीत है।
समसामयिक संदर्भ : आज की राजनीति में “वंदे मातरम्”
वर्तमान राजनीति में “वंदे मातरम्” का विरोध केवल धार्मिक असहमति नहीं, बल्कि राष्ट्रविरोधी विमर्श का हिस्सा बन चुका है। जब कोई राजनीतिक दल या समूह इस गीत का बहिष्कार करता है, तो वह वस्तुतः भारत की अस्मिता को अस्वीकार करता है। ऐसे विरोध का प्रतिकार भावनात्मक नहीं, तर्कपूर्ण होना चाहिए।
सवाल यह नहीं कि कौन “वंदे मातरम्” कहता है या नहीं, बल्कि यह कि कौन भारतमाता का सम्मान करता है और कौन नहीं।
वंदे मातरम् - अस्मिता, एकता और चेतना का प्रतीक
150 वर्षों की यात्रा के बाद भी “वंदे मातरम्” उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में था। यह गीत भारत के आत्मविश्वास, समरसता और मातृत्व भाव का अमर प्रतीक है। आज जब विश्व भारत की ओर आशा से देख रहा है, तब हमें अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को विवादों से नहीं, गौरव से देखना चाहिए।
“वंदे मातरम्” कहना किसी धर्म का उद्घोष नहीं। यह भारत के प्रति प्रेम का संस्कार है। यह हमारी अस्मिता, संस्कृति और आत्मा का गीत है।