इस दुर्भाग्य को झेलने का कोई विकल्प नहीं
17 Jan 2022 21:10:14
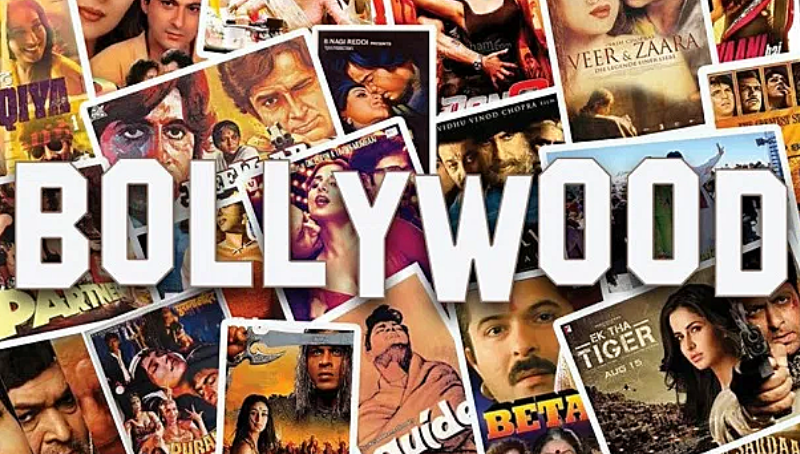
रत्नाकर त्रिपाठी-
इसे "बड़े परदे की बड़ी कंजूसी" कह सकते हैं। या फिर इसको "बड़े परदे की छोटी सोच" की संज्ञा दी जा सकती है। बात यह है कि हिंदी सिनेमा जगत में जनजातीय समुदाय के महान चरित्रों को सतत रूप से उपेक्षा का दंश झेलना पड़ रहा है। यूं भी बॉलीवुड की बीते लंबे समय की जो सोच है, उसमें ऐसे चरित्रों की वहां उपेक्षा के अलावा और कोई अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है।
दुर्भाग्य यह कि इसी हिंदी सिनेमा जगत में विदेशी चरित्र रॉबिन हुड को लेकर भी चित्र बना दिए गये, किंतु भारतीय आदिवासी विभूतियों को सैल्यूलाइड पर महत्व तो दूर, प्रायः कोई स्थान तक प्रदान नहीं किया गया है। कारण स्पष्ट है कि ऐसे नाम अपने बहुत उल्लेखनीय काम के बावजूद फिल्म निर्माताओं तथा वितरकों के लिए "बिकाऊ माल" की श्रेणी में नहीं आ सके हैं। इसलिए उन पर पैसा लगाकर कोई घाटे का सौदा करना नहीं चाहता है।
यह स्थिति दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि भारतीय जनमानस पर सिनेमा का सबसे अधिक असर होता है। यदि इस माध्यम में जनजातीय गौरवों को स्थान दिया जाता तो बहुत अधिक आसानी से देश की बहुत बड़ी आबादी को आदिवासी समाज के यशस्वी अतीत तथा देश एवं धर्म की रक्षा के लिए उनके योगदान से अवगत कराया जा सकता था। लेकिन ग्लैमर की भेड़चाल में यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए यह सोचकर ही संतोष कर लेना चाहिए कि बॉलीवुड ऐसे महान चरित्रों को अपनी सोच तथा कर्म के दायरे से बाहर रखे हुए है। इस बात को दो उदाहरणों से समझिये। बात सन 1982 की है।
तब रिचर्ड एटेनबरो की फिल्म "गांधी" भारत में रिलीज की गयी थी। तब एक स्तंभकार ने लेखन के माध्यम से सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि महात्मा गांधी से जुड़े इतने सशक्त और प्रभावी चित्र का निर्माण एक विदेशी ने किया? क्यों इससे पहले गांधी के देश में ही सिल्वर स्क्रीन पर उन्हें ऐसी किसी फिल्म के माध्यम से स्थान नहीं मिल सका? उन्हीं स्तंभकार ने बड़े-ही चुटीले अंदाज में इस सवाल का खुद ही जवाब भी लिखा था।
उन्होंने लिखा कि यदि कोई भारतीय निर्माता गांधी पर फिल्म बनाता तो उसके साथ यह समस्या होती कि वह बापू को किसके साथ रोमांस करते और पेड़ों के इर्द-गिर्द ठुमके लगाते हुए दिखाता? इस कटाक्ष के जरिये उन लेखक ने यह बताया था कि वस्तुतः हिंदी सिनेमा की रील पर सीधे-सादे गांधी के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए यहां गांधी पर फिल्म बनाना मुनासिब नहीं समझा जाता है।
अब दूसरा उदाहरण। बात दो हजार के दशक के आसपास की है। बॉलीवुड में अचानक शहीद भगत सिंह जी पर फ़िल्में बनाने की होड़-सी मच गयी। लगभग एक ही समय पर अलग-अलग शीर्षकों से इस महान क्रांतिकारी पर चित्रों का निर्माण कर उन्हें प्रदर्शित कर दिया गया। लोग यह देखकर स्तब्ध थे कि इनमें से कुछ सिनेमा में भगत सिंह जी को आजादी के महानायक की बजाय एक रोमांटिक आदमी के रूप में अधिक प्रधानता के साथ चित्रित किया गया था। इन दो उदाहरणों के बाद बॉलीवुड का ऐसा चरित्र देखकर इस बात से संतोष कर लिया जाना चाहिए कि उसके कर्ता धर्ता जनजातीय नायक-नायिकाओं की रियल लाइफ को अपने सर्वनाशी तरीके से रील लाइफ में परिवर्तित करने की बात नहीं सोचते हैं।
गलती केवल फिल्म जगत की नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) केंद्र सरकार की एजेंसी है। इसने बड़ी संख्या में फिल्मों के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान की, किन्तु जनजातीय चरित्रों के देश के लिए योगदान को यह एजेंसी भी कमोबेश पूरी तरह नजरंदाज ही करती रही। जबकि इसी एजेंसी ने बड़ी संख्या में उन फिल्मों के निर्माण का काम किया, जिनमें से अधिकांश की पहचान केवल यह रही कि उनके निर्देशक के रूप में कोई बड़ा नाम इस्तेमाल किया गया। इससे उपजी विचित्र स्थिति को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक समय भोपाल में राज्य सरकार ने एक फिल्म समारोह आयोजित किया। इसमें एक ख्यातिनाम निर्देशक की फिल्म भी प्रदर्शित हुई। स्क्रीनिंग के लिए ये निर्देशक महोदय भी प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित थे। बड़े नाम के चक्कर में फिल्म को देखने भीड़ उमड़ी। लेकिन चित्र के समाप्त होते-होते उस टॉकीज में बमुश्किल डेढ़ दर्जन लोग बचे थे। उनमें भी एनएफडीसी और मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम का स्टाफ तथा वह निर्देशक ही शामिल थे।
मध्यांतर में ही दर्शकों के चले जाने की वजह यह थी कि निर्देशक ने फिल्म को "आप बनाएं, आप ही समझें और आप ही देखें" वाली मनमानी सोच के साथ बना दिया था। एक पत्रकार के रूप में मैंने उन निर्देशक से फिल्म को लेकर दर्शकों की अरुचि पर सवाल पूछा तो उन्होंने पूरी अकड़ के साथ कहा, "मैं मास (भीड़) के लिए नहीं, क्लास के लिए फ़िल्में बनाता हूं। मीडिया या आम दर्शकों के लिए मेरी कोई जवाबदेही नहीं है।" तब मेरे साथ के एक पत्रकार ने कहा, "आपकी जवाबदेही कैसे नहीं बनती है?
आप की इस फिल्म के लिए एनएफडीसी ने पैसा दिया। ये पैसा वो है, जो हम और हमारा परिवार सरकार को टैक्स के रूप में देता है। वह दर्शक भी यह कर अदा करता है, जिसे आप भीड़ बताकर खुद को श्रेष्ठ जताने की कोशिश कर रहे हैं।" निर्देशक महोदय अपना-सा मुंह लिए और बगैर कोई जवाब दिए वहां से खिसक लिए। क्यों नहीं कभी एनएफडीसी ने ऐसी जवाबदेही तय करने की कोशिश की? क्यों ऐसा हुआ कि इस एजेंसी ने अपने पैसे से आदिवासी गौरवों को बड़े परदे पर स्थान दिलाने का शायद प्रयास तक नहींकिया? इनका उत्तर तलाशा जाना चाहिए।
जी हां, मैं भी जानता हूं कि वर्ष 2012 में टंट्या भील पर एक फिल्म बनी थी। लेकिन उसे शायद टॉकीज का मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ। बीच में मैंने सरदार भगत सिंह जी पर एक साथ बनी ढेरों फिल्मों की बात की थी। उससे जुड़ा एक घटनाक्रम है।
जब भोपाल के समाचार पत्रों में अलग-अलग टॉकीजों द्वारा भगत सिंह से जुड़ी अपने-अपने यहां प्रदर्शित फिल्मों के विज्ञापन दिए जा रहे थे, तब एक टॉकीज में फिल्म "कुंवारी दुल्हन" चल रही थी। उस टॉकीज के विज्ञापन में लिखा "सारे भगत सिंह एक तरफ और कुंवारी दुल्हन एक तरफ. " घटना पुरानी है, लेकिन न जाने अतीत के कब से लेकर वर्तमान और आने वाले अनिश्चित समय तक यही टीस सालती रहेगी कि सारे असली नायक एक तरफ और नकली नायक एक तरफ। आदिवासी समाज की महान विभूतियों का देश के लिए टिकाऊ योगदान रहा, लेकिन वो बॉलीवुड के लिए बिकाऊ नहीं रहे, इस दुर्भाग्य को ढोने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है।